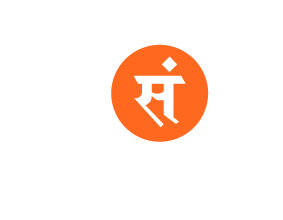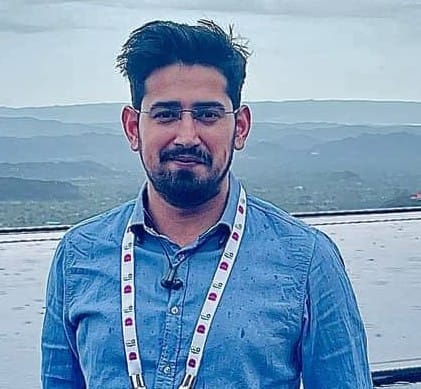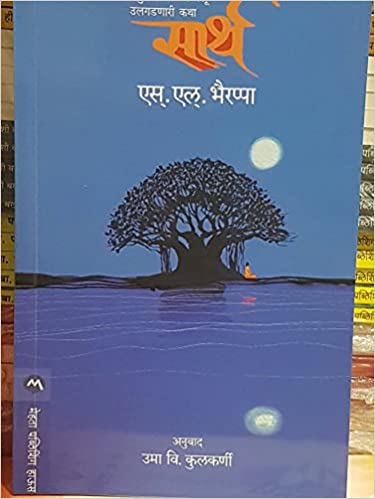
इतिहास और वर्तमान के भ्रमों की यात्रा है... सार्थ
सार्थ : एस. एल. भैरप्पा का कन्नड़ भाषा में रचित सुप्रसिद्ध उपन्यास है। भारत के मध्यकालीन सामाजिक ऊहापोह, विचलन, विभिन्न मत-मतान्तरों का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास का कालखण्ड सातवीं-आठवीं शताब्दी का भारत है। उस समय वैदिक धर्म का प्रभाव और उसका अनुपालन सीमित, संशयग्रस्त हो चला था। बौद्ध मत को राजकीय संरक्षण में प्रमुख मान्यता मिल रही थी। वृहत्तर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत सिंध की ओर से अरबों ने तलवार, हिंसा के बल पर इस्लाम को फैलाना शुरु कर दिया था। निराशा का वातावरण फैलने लगा था।
नैराश्य की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि पाठक को उपन्यास के पहले ही पृष्ठ पर यह पता चले कि वह नायक जिससे पाठक का अभी परिचय नहीं हुआ हो, उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी राजा से सम्बन्ध बना लेती है और उस अनुचित सम्बन्ध से एक पुत्र भी हो जाता है। विषाद, सामाजिक बहिष्कार, अपयश,कुल की बदनामी को सोचती नायक की माँ की मृत्यु हो चुकी हो और दूर कहीं नायक को मृत्यु का समाचार मिले। पाठक किस प्रकार उस नागभट्ट में अपने नायक को देखेगा? लगभग उपन्यास के अंत तक बदले की भावना से ग्रस्त और प्रेम से वंचित नायक नागभट्ट वासना में फिसलता, मोह में गिरता-पड़ता, अवगुंठन में जीता आगे बढ़ता है। बौद्ध मत, वामाचार, योग के रास्ते पकड़ता-छोड़ता भगवान कृष्ण के जीवन चरित को अभिनीत करके पुनः स्वधर्म की और लौटता है। इसका कथानक प्रथम पुरुष में है। नायक की आँखों से कहानी घटित होती है। मध्यकालीन भारत की स्थिति का सूक्ष्म चित्रण मिलता है सार्थ में। बौद्ध मत के प्रचार-प्रसार,उसके ऐश्वर्य के सामने वैदिक धर्म किस प्रकार अपनी निष्ठा और नियम खोता जा रहा है? उस समय का नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा, उसके उन्नयन के लिए ही प्रतिबद्ध था। फिर भी समाज में वेद, उपनिषद,राम-कृष्ण आदि के चरित्र इतने गहरे थे कि सनातन का उच्छेदन आसान नहीं था।
बहुत बारीकी से भैरप्पा जी ने उपन्यास के माध्यम से यह भी बताया कि किस प्रकार 'आचार्य वज्रपाद' जैसे बौद्ध गुरु ने आम जनता पर प्रभाव डालने के लिए वैदिक-पौराणिक चरित्र के गठन, मुद्राएँ, देवप्रतिमा विज्ञान के लक्षणों को बोधिसत्व की प्रतिकृति के साथ जोड़कर, बलपूर्वक चित्रण करवाया, जोकि आज भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है जैसे भगवान विष्णु के सदृश अवलोकितेश्वर, शिव के सदृश मंजुश्री और दुर्गा के सदृश तारा का विग्रह निर्माण।
लगभग तीन सौ पृष्ठों तक फैली यह कृति जीवन के सभी पक्षों को छूती है। नागभट्ट और नटी चन्द्रिका के बीच प्रेम की धारा कथा को सरस बनाती है। नागभट्ट प्रेम करके भी हठ से चन्द्रिका को पाना चाहता है दूसरी ओर चन्द्रिका, जो संगीत की साधिका है, जो अपने जीवन में कितनी ही विसंगतियों, वासनाओं के खड्ड से निकलकर ध्यान मार्ग पर चल पड़ी है, केवल शुद्ध, सात्विक प्रेम करना चाहती है नागभट्ट से,दाम्पत्य जीवन नहीं। वह गणिका नहीं है।सार्थ के चन्द्रिका से बहुत कुछ समानता मिलती है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास 'बाणभट्ट की आत्मकथा' की निपुणिका (निउनिया)से। निपुणिका भी अपने प्रणय की बात कभी भी बाणभट्ट से प्रत्यक्ष नहीं कहती। बाणभट्ट(सूत्रधार की भूमिका में) के प्रथम नाटक मंचन से ही बाण के प्रति प्रेम लिए, तमाम अवरोधों के बाद बाण के नाटक में प्रेम दग्ध हृदया का अभिनय करते हुए सचमुच मंच पर ही अपनी आहुति दे देती है। वहीं सार्थ की नायिका अपने नागभट्ट को पतन से उठाने के लिए निषिद्ध तंत्राचार की योनि पूजा को भी स्वीकार करती है। उसका त्याग बहुत बड़ा है। राष्ट्र को जगाने के लिए अरब म्लेच्छों के कब्जे वाले पश्चिमोत्तर भाग मूलस्थान में नागभट्ट-चन्द्रिका दोनों नाटक खेलते हैं। दोनों पकड़ लिये जाते हैं। उन पर अत्याचार होता है। उससारा म्लेच्छों द्वारा पाशविक व्यवहार, बलात्कार और उस पिशाचवृत्ति का बीज न चाहते हुए अपने गर्भ में धारण करती है।नागभट्ट भी उसकी पवित्रता को स्वीकारता है क्योंकि वह स्वयं वासना मुक्त हो भारती देवी के एक वाक्य में उसे बोध होता है-- "गृहस्थाश्रम और वैवाहिक जीवन एक व्रत है। भावना को व्रत के नियम के अनुकूल ढ़ालना उत्तम व्रत ही नहीं बल्कि यह कर्ममार्ग का मूल तत्व है।"
इसमें ऐतिहासिक चरित्र आदि गुरू शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती देवी भी हैं। हालाँकि आज भी कतिपय विद्वान शंकराचार्य का समय ईसा पूर्व लगभग दूसरी शती मानते हैं परन्तु उपन्यासकार ने इनका समय आठवीं शती मानकर रचना की है। मंडन मिश्र-भारती देवी और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ कहीं भी बोझिल नहीं करता बल्कि तत्कालीन समय के विश्रृंखल समाज और देशकाल, गृहस्थ और सन्यास को एक सुनिश्चित दिशा देते हुए ज्ञानमार्ग की प्रतिस्थापना होती है। आगे देश को बहुत कुछ सहना था, मंदिर-स्थापत्य-वैदिक-बौद्ध आदि सब पर म्लेच्छों का प्रहार होना था। बचाने लायक केवल सात्विक गृहस्थ धर्म ही था शायद इसीलिए भैरप्पा जी ने गृहस्थ होने और वीर्यवान संतति को जन्म देने के महागुरू के आशीर्वाद के साथ ही अपनी लेखनी को रोक दिया।
नारी चरित्र की दृष्टि से इस कृति में दो प्रमुख पात्र हैं, प्रथम भैरप्पा जी की सृजित 'चन्द्रिका' और दूसरी ऐतिहासिक चरित्र 'भारती देवी'। चन्द्रिका पूरे उपन्यास में कलाआराधिका होते हुए, योग को साधते हुए प्रेम को सात्विक भाव में पाने का प्रयत्न करती है।विकट परिस्थितियों में शीलभंग होने के बाद भी ध्यानयोग से स्वयं को परिशुद्ध कर अद्भुत् धैर्य रख कर भविष्य गृहस्थयोग की ओर उन्मुख होती है जिसमें नायक नागभट्ट की भी प्रत्याशा होती है। तथाकथित प्रगतिशीलता के चलताऊ पुरुष अहंकार से दूर स्वीकार्य भाव सृजित कर लेखक नायकत्व को स्थापित करता है। दूसरी ओर भारती देवी अपने ज्ञान-कौशल से प्रखर शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में अतिरिक्त समय माँगने पर विवश कर देती है। थोड़े ही पन्नों पर भारती देवी का चरित्र आया है परन्तु उनका संवाद न केवल उस समय बल्कि आज भी प्रेम और परिवार की मर्यादा और कर्तव्य को पुर्नस्थापित करता है।
नायक निर्बन्ध, उद्दाम, शारीरिक आकर्षण को प्रेम का उद्गम लक्ष्य करके, बार-बार प्रश्न पूछ कर मानो आज के युवाओं को समाधान देता है।
मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में हारने के बाद, सन्यास लेने के निर्णय पर बिना विचलित हुए निष्ठापूर्वक गृहस्थधर्म के पालन की प्रतिबद्धता, उनका त्याग सन्यास से कहीं ऊँचा सिद्ध कर देती हैं। उनसे प्रेरणा लेकर ही नायक गृहस्थ की महत्ता को समझता हुआ चन्द्रिका के साथ भविष्य खोजता है।
तत्कालीन भारत की अनेक समस्याओं से जूझते निराश समय की परिणति लेखक दो तरह से करता है। सैद्धांतिक स्तर पर शंकराचार्य के ज्ञानमार्ग की प्रतिष्ठा द्वारा सनातन की प्रतिष्ठा और कर्ममार्गी भारती देवी की सात्विक गृहस्थ व्रत द्वारा परिवार की प्रतिष्ठा। मानों लेखक स्वयं नागभट्ट के रुप में विसंगतियों के बीच रास्ता खोजने निकला है तभी तो सारी कथा नायकमुख द्वारा आगे बढ़ती है। कथानक घटना दर घटना इस तरह आगे बढ़ती है कि आप इसे पूरा करही चैन लेते हैं।
तत्कालीन मध्ययुग की लड़ाईयों और धर्मभीरुता की वृत्ति के चलते किस तरह से भारत को भविष्य में इस्लामिक आक्रमण से आक्रांत होना है,इसका स्पष्ट चित्रण सार्थ में मिलता है। प्रतिहार सैनिक मजबूत एवं संख्या में भी अधिक होने के बावजूद मूलस्थान को अरब आक्रांता से छुड़ाने के लिए मात्र इसलिए नहीं लड़ते कि म्लेच्छों ने यह बात फैला दी थी कि यदि प्रतिहार सेना आक्रमण करती है तो मार्तण्ड मंदिर नष्ट कर दिया जायेगा। "कहीं मेरे कारण मंदिर न टूट जाय.." यह सोच कर बिना अन्य कोई रणनीति बनाये जीता हुआ मोर्चा छोड़कर दूसरी ओर चली जाती है। इस तरहकितनी ही लड़ाईयाँ भारत हारा है इतिहास में।
सार्थ, धर्म, प्रेम और परिवार की कहानी है जिसमें नायक प्रेम को शरीर में खोजते हुए, धर्मच्युत होकर देशकाल के संकीर्ण धार्मिक व्यामोह में फँसता हुआ, आसमानी किताबों के रहनुमाओं के घृणित अमानवीय अत्याचारों से निकलकर पुनः सदगृहस्थ की ओर बढ़कर सनातन मूल्यों की प्राप्ति करता है।