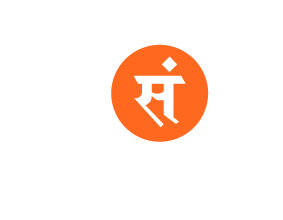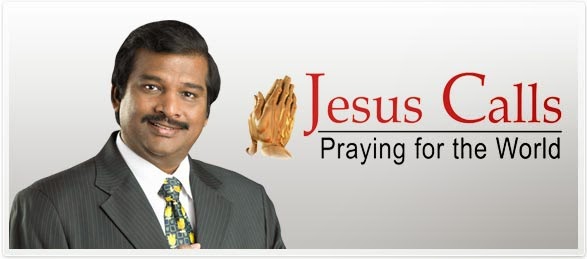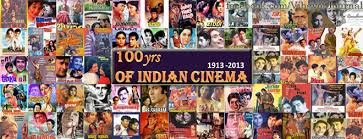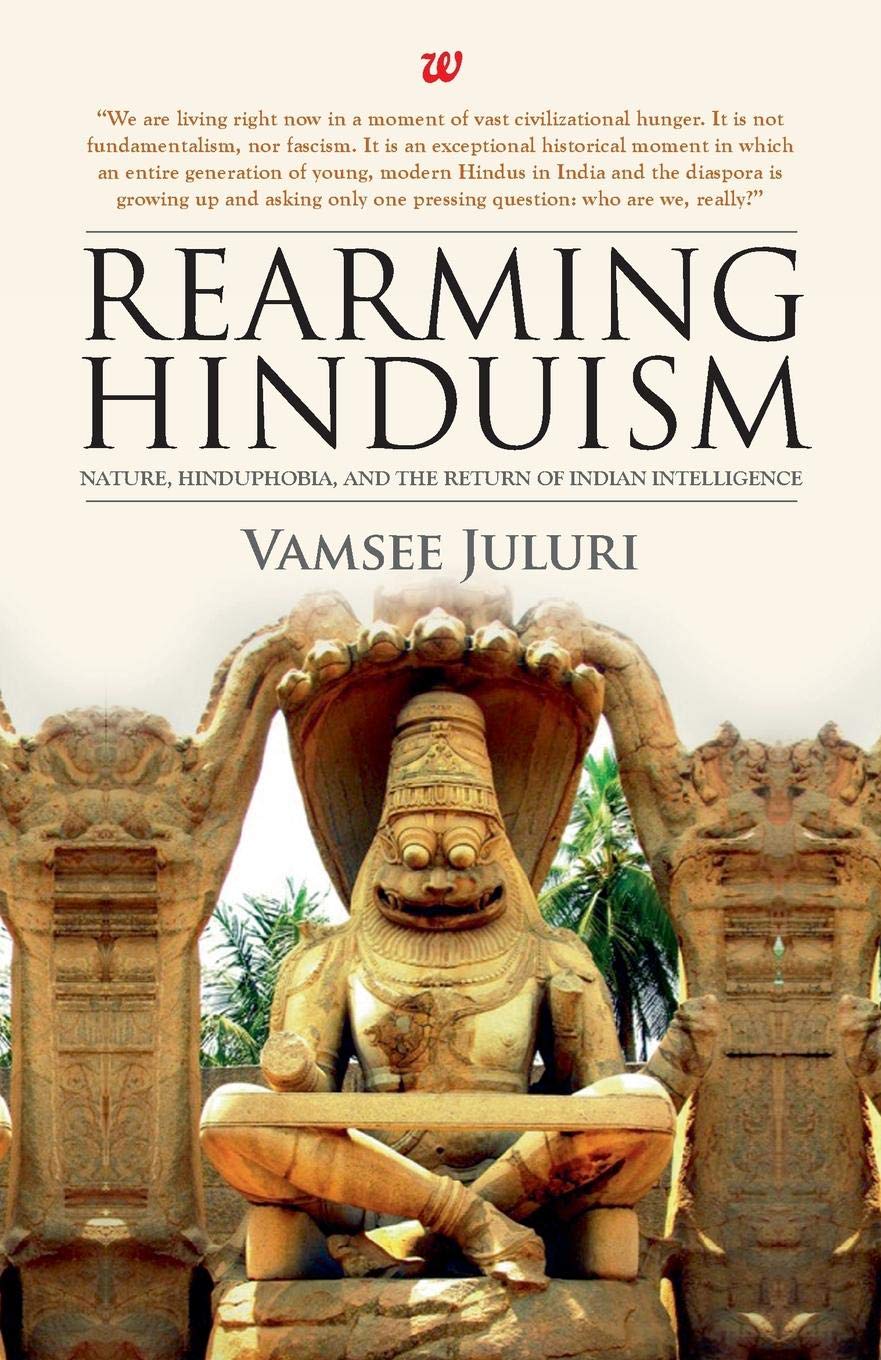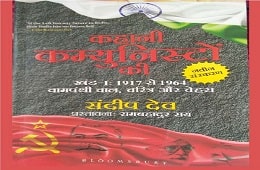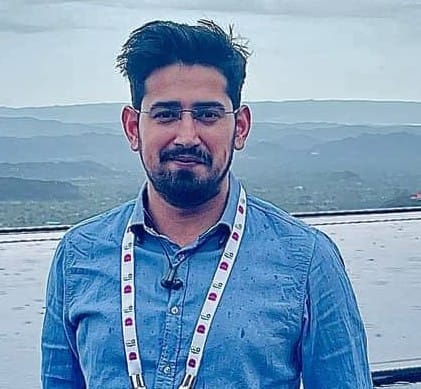रॉकेट्री: फिल्म जो कहा गया, उसे ध्यान से सुनना है और जो नहीं कहा गया, उसे ध्यान से समझना है
फिल्म रॉकेट्री में नम्बी नारायणन अपने साथ फ्रांस जा रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वहां पर काम करने का एक टिप्स देते हैं कि वहां पर जो कुछ कहा जाए उसे ध्यान से सुनना है और जो कुछ न कहा जाए, उसे ध्यान से समझना है। भारतीय वैज्ञानिक इसी टिप्स के आधार पर काम करते हैं, कम बोलते हैं और वहां से बहुत कुछ सीखकर वापस आते हैं। ऐसा लगता है कि यह पूरी फिल्म भी इसी संवाद के आधार पर गढ़ी गई है। कुछ मुद्दों को साफगोई के साथ परदे पर कहा गया है और कुछ अतिशय संवेदनशील मुद्दों की तरफ केवल संकेत भर किया गया है। ऐसी घटनाओं की पूरी पृष्ठभूमि समझने और सही निष्कर्ष निकालने का कार्य दर्शकों पर छोड़ दिया गया है।
उदाहरण के लिए नम्बी नारायणन को फर्जी केस में फंसाने के बाद उन पर हुए अत्याचार को बहुत मार्मिक तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म यह भी रेखांकित करने में सफल रही है कि नम्बी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय अंतरिक्ष अभियान कैसे दशकों पीछे चला गया। लेकिन नम्बी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, उसकी परतों को फिल्म ठीक ढंग से नहीं खोल पाती। शायद, इसमें एक विचारधारा का पोल खुलने का डर था और उस अधिकारी पर अंगुली उठने का डर था, जिसे गुजरात दंगों के दौरान गलत साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। उस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद नम्बी नारायणन ने खुलकर यह बात कही थी कि गुजरात दंगों की तरह ही उस अधिकारी ने इसरो केस में मनगढंत कहानियां गढ़ी और उसे सनसनीखेज ढंग से परोसा। नम्बी नारायणन ने आगे कहा कि जब वह गिरफ्तार हुआ तो मैं बहुत खुश था क्योंकि वह हमेशा इसी तरह की शरारतों में संलिप्त रहता था। इस तरह की चीजों का अंत होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं।
वह अधिकारी हाल ही में तीस्ता सीतलवाड़ के साथ गिरफ्तार हुआ है। जाहिर है इस लॉबी के पास मजबूत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समर्थन होगा। इस अधिकारी पर यदि खुलकर प्रश्न उठता तो गुजरात दंगों के दौरान उसके द्वारा निभाई गई भूमिका और भी संदिग्ध बन जाती। शायद, इसीलिए यह फिल्म नम्बी के खिलाफ एक बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की तरफ संकेत तो करती है, लेकिन उसके किरदारों की जांच-पड़ताल करने से बचती है। फिल्मांकन की इस शैली के कारण राकेट्री अपने साथ कई प्रश्न लेकर आती है। एकाध प्रश्नों का उत्तर भी देती है, लेकिन अधिकांश अनुत्तरित रह जाते हैं। इसीलिए दर्शक मन में एक टीस और कई सारे प्रश्न लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है।
इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें किसी भी तरह की अतिरंजना नहीं है। फिल्म के अंतिम दृश्य में जब नम्बी नारायणन से यह कहा जाता है कि वह सभी को माफ कर दे तो उनका यह उत्तर की माफी देने से मामला समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि यह हल्का हो जाएगा। किसी और के साथ मेरे जैसी दुर्घटना न हो, इसके लिए माफी नहीं लड़ना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से यह कथन सहज है और सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सही भी। नम्बी के चरित्र को इसी तरीके से पूरी फिल्म में मानवीय बनाए रखा गया है। अमेरिका में इच्छित प्रोफेसर के अधीन काम करने के लिए उनके द्वारा घरेलू काम करने की बात हो या रूसी और अमेरिकी महिला सहकर्मियों से उनके संवाद हो, बहुत ही सहज और भारतीय मन के करीब लगते हैं।
फिल्म स्वतंत्रता के बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी और उसकी चुनौतियों को सलीके से परोसती है। वैज्ञानिकों ने जिस जज्बे के साथ एक सकारात्मक संस्कृति के संस्थान बनाए, और जिस सृजनात्मकता के साथ चुनौतियों पर विजय पायी, राकेट्री को बखूबी परदे पर उतारती है। यह फिल्म भी उन्ही वैज्ञानिकों की तरह विविध पक्षों को साधती हुई दिखती है। शाहरूख खान की छवि का इस्तेमाल करना हो या फिल्म के अंत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंगल मिशन के बाद के सम्बोधन और 2019 के पद्मभूषण के समय के विजुअल्स का उपयोग करना, यह दर्शाता है कि फिल्म और निर्देशक देशभक्ति की एक कहानी सुनाने में ज्यादा उत्सुक थे और इसके लिए उन्होंने सभी तरह की छवियों का इस्तेमाल किया।
राकेट्री से पहले सोनी लाइव पर राकेट ब्वायज वेबसीरीज भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन और संघर्ष तथा अंतरिक्ष और सुरक्षा चुनौतियों को परदे पर दिखा चुकी है लेकिन रॉकेट्री पहली ऐसी फिल्म है, जिसमें बड़े परदे पर एक वैज्ञानिक के जीवन और भारत की अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को एकसाथ दिखाया गया है। खिलाड़ियों और गैगस्टरों से हटकर वैज्ञानिकों के जीवन में निर्देशकों की रूचि भारतीय दर्शकों और समाज में आ रहे बदलावों की तरफ भी संकेत करता है। इस बदलाव को स्वर देने वाली इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए।
…