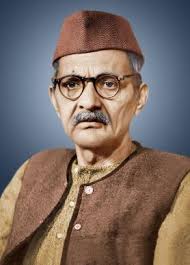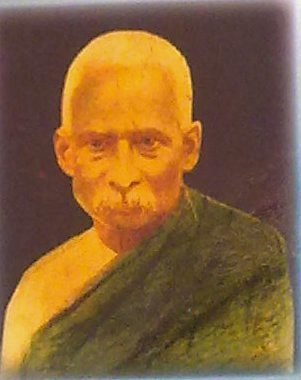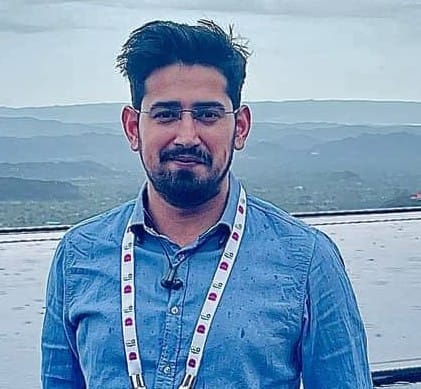कट-कट मुंड गिरैं ज्वानों के, उठ-उठ रुंड करें तलवार। यह गति हो गई रणखेतों में, बहने लगी खून की धार। आल्ह खंड की ये पंक्तियां न सिर्फ काव्य के वीर रस को नई ऊंचाइयां देती मालूम पड़ती हैं बल्कि भारत के इतिहास को भी बेहद सरल और रोचक शब्दों में दोहराती हैं। एक दौर में हिंदी पट्टी के बड़े क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय रहे आल्ह खंड को यदि हम भारत में सबसे प्रभावशाली लोकसंवाद का माध्यम कहें तो कुछ गलत न होगा। 12वीं सदी के महोबा के चंदेल शासक परमाल के सेनापति भाईयों आल्हा-ऊदल की कहानी सुनाने वाला आल्ह खंड करीब 1000 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी रिसते हुए यहां तक पहुंचा है। कोई विधिवत ग्रंथ न होने और अकादमिक इतिहासकारों की नजर से उपेक्षित होने के बाद भी यदि आज यह कहानी सुनकर श्रोताओं की भुजाएं फड़कती हैं तो यह आल्ह खंड की संवादपरकता की ही मिसाल है।
साहित्य के मर्मज्ञ मानते हैं कि आल्हखंड की रचना परमाल के दरबारी कवि जगनिक ने की थी। हालांकि वह रचना अप्राप्य है, लेकिन उसके आधार पर ही देश के हिंदी भाषी क्षेत्र में आल्ह खंड की कई शैलियां प्रचलित हैं। मूल रूप से यह अवधी-बुंदेली मिश्रित शैली में है और सिर्फ काव्य रूप में ही है। मध्य प्रदेश की बघेली बोली, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी और उत्तर बिहार की मैथिली बोली में भी आल्हा का काफी प्रचार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में भी आल्हा लोक बोली में गूंजता है। क्षेत्र के विस्तार के साथ आल्हा के गायकों की बोली बदल जाती है, वाद्य यंत्रों में कुछ अंतर दिखता है, लेकिन संदेश एक ही है। आमतौर पर इसे ढोल, मंजीरे और खंजड़ी के साथ गाया जाता है।
आल्हा की लोकप्रियता और प्रभाव को यूं भी समझ सकते हैं कि भारत से होते हुए यह ब्रिटेन तक पहुंचा है, जहां इस पर काफी शोध हुए हैं और साहित्य भी लिखा गया है। आल्ह खंड के एक हिस्से 'ब्रह्मा का विवाह' का अंग्रेजी में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'The Lay of Brahma's Marriage: An Episode of the Alh-Khand' शीर्षक से अनुवाद किया है। आयरिश मूल के ग्रियर्सन 19वीं सदी में भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत ब्रिटिश शासन के लिए काम कर रहे थे। हालांकि उनकी भारतीय भाषाओं और लोककलाओं में गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने आल्ह खंड के इस हिस्से का अनुवाद किया था। सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारी सर चार्ल्स इलियट ने आल्हा को लिपिबद्ध कराने का काम किया था।
आल्हखंड को लिपिबद्ध किए जाने का किस्सा भी बेहद रोचक है। 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर रहे अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट की मुलाकात कुछ अल्हैतों (आल्हा गायन करने वाले) से हुई थी। आल्हा सुनकर इलियट मंत्रमुग्ध हो गए और फिर उनकी रुचि ऐसी बढ़ी कि उन्होंने एक गवैये को नौकरी पर ही रख लिया और उससे 'आल्ह खंड' के प्रचलित सभी किस्सों को लिपिबद्ध कराया। इलियट के प्रयास से 23 खंडों का आल्हा प्रकाशित हुआ। इसके बाद फिर कई प्रयास हुए और आज आल्ह खंड की कई रचनाएं उपलब्ध हैं। उनके अलावा एक और ब्रिटिश अफसर विलियम वाटरफील्ड ने 1860 में ‘Lay of Alha’ शीर्षक से आल्ह खंड के हिस्से का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उनकी इस रचना को इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया था। बंगाल और बिहार में प्रशासक के तौर पर काम करने वाले सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आल्ह खंड की लोकप्रियता को लेकर लिखा है कि पटना से दिल्ली के बीच में इससे लोकप्रिय कथा कोई दूसरी नहीं है।
'आल्ह खंड' के विस्तार में जाने से पहले हमें इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और किरदारों के बारे में भी जानना होगा। बुंदेलखंड में स्थित महोबा पर 12वीं सदी में चंदेल राजपूत वंश के राजा परमाल देव का शासन था। उनके सेनापति थे, आल्हा और ऊदल। दोनों ही सगे भाई थे और बनाफर राजपूत थे। इन दोनों की वीरता पर ही राजा परमाल देव के दरबार में कवि जगनिक ने आल्ह खंड की रचना की थी। भले ही उनकी यह रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनश्रुतियों में ऐसी व्याप्त है कि उनके संकलन से ही कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। राजा परमाल देव और आल्हा ऊदल दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। आल्ह खंड में कुल 52 हिस्से हैं और हर हिस्से में युद्ध का वर्णन है, जिसमें आल्हा और ऊदल की वीरता का बखान किया गया है। इसके अलावा आल्हा ऊदल के मौसेरे भाई मलखान एवं सुलखान और राजा परमाल देव के बेटे ब्रह्मा अहम किरदार हैं।
आल्ह खंड में राजा परमाल की पत्नी मलहना के भाई माहिल का नकारात्मक किरदार चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि राजा परमाल देव ने महोबा के राजा बासुदेव परिहार को परास्त कर महोबा पर जीत हासिल की थी और फिर उनकी बेटी मलहना से स्वयं विवाह किया था। इसके अलावा उनकी दो अन्य बेटियों देवला और तिलका का विवाह अपने दो बनाफर राजपूत सेवकों क्रमश: दसराज और बच्छराज से करा दिया था। इन्हीं दसराज के बेटे आल्हा और ऊदल थे। ऊदल को उदय सिंह भी कहा जाता है। इसके अलावा तिलका और बच्छराज के पुत्र थे, मलखान और सुलखान। महोबा पर भले ही परमाल का शासन था, लेकिन बुंदेलखंड के ही उरई के शासक और बासुदेव परिहार के बेटे माहिल को यह कभी स्वीकार नहीं था। उसे हमेशा यह लगता था कि परमाल देव ने महोबा को उनके पिता को हराकर जीता है और उसके वास्तविक अधिकारी वह हैं। कहा जाता है कि इसी के चलते वह अकसर ऐसे कुत्सित प्रयत्न करते थे कि महोबे की सेना किसी युद्ध में रत रहे। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में माहिल के बेटे अभय सिंह ने भी हिस्सा लिया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था।
आल्ह खंड के बारे में बात करते हुए महोबा नगर के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसके इर्द-गिर्द यह पूरा काव्य रचा गया है। महोबा को महोत्सव नगर के नाम से चंद्रवर्मन उर्फ नन्नुक ने स्थापित किया था, जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रवर्मन को ही चंदेल राजवंश का संस्थापक माना जाता है। चंदेलों से पहले यहां गहरवार और प्रतिहार राजपूतों का शासन था। पन्ना के चंद्र वर्मन ने प्रतिहार शासकों को परास्त कर महोबा पर सत्ता कायम की थी और इस शहर को स्थापित किया था। उनके बाद कई और प्रतापी चंदेल शासक हुए, जिनमें प्रमुख नाम विजयी-पाल (1035-1045 ई.) और कीर्तिवर्मन (1060-1100 ई.) का है। कीर्तिवर्मन ने कीरत सागर झील का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और आल्हा-ऊदल के बीच पहली लड़ाई इस कीरत सागर के नजदीक ही हुई थी। आज भी इस कीरत सागर का महोबा में अस्तित्व मिलता है। कीर्तिवर्मन के बाद मदन वर्मन प्रमुख शासक थे, जिनका शासन 1128-1164 ई. के बीच रहा। इनके बाद राजा परमाल के हाथों में महोबा की सत्ता की बागडोर चली गई थी, जिनके सेनापति आल्हा-ऊदल थे। आज भी महोबा में चंदेल राजपूतों का बाहुल्य है, जिससे यह पुष्टि होती है कि एक दौर में चंदेल वंशी राजपूतों का प्रभुत्व रहा होगा।
जब आल्हा-ऊदल से परास्त हुई पृथ्वीराज की सेना
आल्हा ऊदल की वीरता को इससे आंका जा सकता है कि जिन पृथ्वीराज चौहान का भारत के इतिहास में अप्रतिम वीरता के लिए जिक्र किया गया है, उनकी सेना भी इन दोनों भाईयों से युद्ध में मात खाकर लौट गई थी। पृथ्वीराज चौहान और महोबा की सेना के बीच पहले युद्ध की कहानी भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना एक बार तुर्की सेना का पीछा करते हुए राह भटक गई थी। सेना में पृथ्वीराज चौहान के अलावा उनके सेनापति चामुंडाराय भी मौजूद थे। किवदंती है कि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने परमाल की पत्नी मलहना की सुंदरता के बारे में सुना तो रीझ गया और महोबे पर हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में महोबा के सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी और आल्हा ऊदल के नेतृत्व में चौहान की सेना को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया।
परमाल के बेटे पर मोहित थी पृथ्वीराज की पुत्री बेला
एक किवदंती है कि बनाफर राजपूतों को क्षत्रिय समाज में कमतर माना जाता था और कोई भी उनसे अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहता था। ऐसे में हर विवाह में लड़ाई का जिक्र है और विजेता होने के पश्चात ही विवाह संपन्न होता है। आल्हा का विवाह हो या फिर उनके छोटे भाई ऊदल का विवाह, इन सभी का फैसला युद्ध के जरिए ही हुआ था। कहा यह भी जाता है कि आल्हा और ऊदल की वीरता के चलते एक बार पृथ्वीराज चौहान की सेना भी पीठ दिखाकर भाग गई थी। हालांकि दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान से जंग में ही राजा परमाल की सेना पराजित हुई थी। यह जंग में विवाह के चलते ही हुई थी। किवदंती के अनुसार राजा परमाल के बेटे ब्रहमा पर पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला मोहित हो गई थी और दोनों ने गुपचुप विवाह कर लिया था। यह बात पृथ्वीराज को स्वीकार नहीं थी और उसने दोनों को कभी मिलने नहीं दिया।
पृथ्वीराज से युद्ध में ऊदल को मिली वीरगति
पृथ्वीराज ने महोबे पर हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान ताहर ने ब्रह्मा को घायल कर दिया, दूसरी ओर क्रोध में ऊदल ने ताहर का वध कर दिया। ब्रह्मा की मृत्यु हो गई और बेला सती हो गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। कहा जाता है कि इस युद्ध में ऊदल की मृत्यु हो गई थी। यही नहीं अप्रतिम योद्धा कहे जाने वाले मलखान और सुलखान को भी इस युद्ध में वीरगति मिली थी। इसके बाद अपने भाई से अतिशय प्रेम करने वाले आल्हा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ संप्रदाय अपना लिया था। कई स्रोतों के मुताबिक आल्हा-ऊदल का पृथ्वीराज चौहान से दूसरा युद्ध 1182 में हुआ था, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 में मोहम्मद गोरी से जंग में हुई थी। किवदंती है कि ब्रह्मा की युद्ध में मौत के बाद उसकी पत्नी बेला भी उसकी चिता के साथ ही शहीद हो जाती है। इस प्रसंग को बेहद दुख के साथ गाते हुए अल्हैत कहते हैं-
सावन सारी सोनवा पहिरे, चौड़ा भदई गंग नहाय, चढ़ी जवानी ब्रह्मा जूझे, बेलवा लेई के सती होइ जाय।
52 खंडों में है आल्हा
आल्हा की शुरूआत पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता के स्वयंवर से होती है, अलग-अलग भाग में अलग-अलग कहानियां हैं, ज्यादातर भाग में युद्ध ही है। आखिरी भाग में महोबा की राजकुमारी बेला के सती होने की कहानी है। आल्हा में कुल 52 खंड हैं, जिनमें से प्रमुख हैं- परमाल का विवाह, महोबा की लड़ाई, गढ़ माड़ों की लड़ाई, नैनागढ़ की लड़ाई, विदा की लड़ाई, महला-हरण मलखान का विवाह, आल्हा की निकासी, लाखन का विवाह, बेतवा नदी की लड़ाई, लाखन और पृथ्वीराज की लड़ाई, बेला सती आदि।
वीर रस से पूर्ण है आल्ह खंड, अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग
आल्ह खंड की रचना की गहराई से विवेचना करें तो इस में अतिशयोक्ति अलंकार का काफी प्रयोग किया गया है। किसी भी एक दृश्य का चित्रण करने से पहले लंबी भूमिका सहारा लिया गया है । जैसे पृथ्वीराज और महोबा की सेना की लड़ाई का प्रसंग कवि ने इन शब्दों में किया है-
ना मुंह फेरैं, महोबे वाले, ना ई दिल्ली के चौहान।
कीरतसागर मदनताल पर, क्षत्रिन कीन खूब मैदान।
कटि कटि गिरैं बछेड़ा, चेहरा गिरैं सिपाहिन केर,
बिना सूंढ़ि के हाथी घूमैं, मारें एक एकको हेर।
चौड़ा ऊदल का रण सोहै, धांधूं बनरस का सरदार,
सवापहर लों चली सिरोही, नदिया बही रक्त की धार।
आल्हा के कीरत सागर की लड़ाई खंड के इस काव्य का अर्थ है- न महोबे के सैनिक पीछे हटने को तैयार हैं और न ही दिल्ली के चौहान पीछे हट रहे हैं। कीरत सागर और मदनताल पर क्षत्रियों के बीच घमासान युद्ध देखने को मिलता है। युद्ध में शामिल बैल, घोड़े और हाथियों के सिर कटकर गिरते हैं। सिपाहियों के सिर धड़ अलग होकर गिर रहे हैं। बिना सूंड़ के हाथी रण क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऊदल और पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडाराय का युद्ध देखते ही बनता है। देर शाम तक लड़ाई चलती है और नदी में रक्त बह निकलता है। कवि ने जिन शब्दों में युद्ध का चित्रण किया है, उनसे वीर रस का संचार होता है।
इसी प्रकार पहले खंड संयोगिता स्वयंवर को भी कवि ने बेहद रोचक शब्दों में प्रस्तुत किया है। राजा जयचंद की छटा, उसके आसन और दरबार का सुंदर का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा-
राजा जयचंद कनउज वाला, आला सकल जगत सिरनाम।
को गति बरनै त्यहिमंदिर कै, सो है सोन सरिस त्यहिधाम।
केसरि पोतो सब मंदिर है, औ छति लागि वनातन केर।
सुवा पहाड़ी तामें बैठे, चक्कस गड़े बुलबुलन केर।
लाल औ मैनन कै गिनती ना, तीतर घूमिरहे सब ओर।
पले कबूतर कहुं घुटकत हैं, कहुं-कहुं नाचि रहे हैं मोर।
लागि कचहरी है जयचंद कै, बैठे बड़े-बड़े नरपाल।
बना सिंहासन है सोने का, तामें जड़े जवाहिर लाल।
तामें बैठो महाराज है, दहिने धरे ढाल तलवार।
कन्नौज का राजा जयचंद पूरे जगत में सिरमौर है। उसके राज्य के मंदिर की महिमा कही नहीं जा सकती, जो पूरी तरह स्वर्णजड़ित है। केसर से पुते मंदिर में तोते, बुलबुल, मैना और तीतरों की आकृतियां बनी हैं, जिनकी शोभा देखते ही बनती है। कहीं बेशुमार कबूतर बने हैं तो कहीं नाचते मोरों की आकृति है। सोने के बने और जवाहरों से जड़े सिंहासन पर ढाल तलवार लिए बैठे राजा जयचंद के दरबार में बड़े-बड़े राजा बैठे हैं।
आल्ह खंड को लेकर क्या कहते हैं आचार्य़ रामचंद्र शुक्ल
आल्ह खंड की रचना करने वाले कवि जगनिक के बारे में कहा जाता है कि वह परमाल देव के दरबारी कवि थे। जनकवि जगनिक नाटक के रचयिता डॉ. कुंवर चंद्रप्रकाश सिंह ने लिखा है कि जगनिक और आल्हा के छोटे भाई ऊदल बचपन में ही निराश्रित हो गए थे। इसके बाद उन्हें राजा परमाल की पत्नी मलहना ने ही अपने पुत्र के समान पाला था। भले ही जगनिक परमाल के दरबार में कवि थे, लेकिन मलहना उनके लिए मां के समान थीं। इस बात को इससे भी बल मिलता है कि तमाम शोध ग्रंथों और लेखकों ने जगनिक के परिवार की पुष्टि नहीं की है। यहां तक कि उनकी जाति को लेकर भी लेखक एकमत नहीं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में कवि जगनिक को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, 'ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहां जगनिक नामक भाट थे, जिन्होंने महोबा के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का वर्णन काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके गीतों का प्रचार पूरे उत्तरी भारत में हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं अता-पता नहीं है, लेकिन उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं।' रामचंद्र शुक्ल ने जगनिक को वीर गाथा काल के महत्वपूर्ण कवियों में शामिल किया है।
सावन में आल्हा सुनने का है प्रचलन, इससे भी जुड़ी है एक कहानी
दरअसल चंदेल वंश के 15वें शासक परमाल के राज्य महोबा पर पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने उस समय हमला किया था, जब रानी मलहना रक्षाबंधन के मौके पर कीरतसागर में पूजा के लिए जा रही थी। इसके जवाब में आल्हा-ऊदल के नेतृत्व में महोबे की सेना ने वीरता से युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज की सेना को भागना पड़ा। कहा जाता है कि यह लड़ाई तीन दिन तक चली थी। आज भी इस दिन के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन के तीसरे दिन महोबा में कजली महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन महोबा के लोग कीरत सागर के नजदीक स्थित गोखर हिल में जाकर गजांतक शिव की पूजा करते हैं।
…

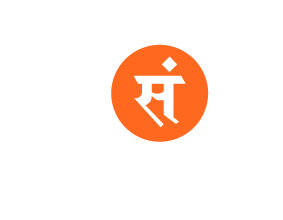



.jpeg)